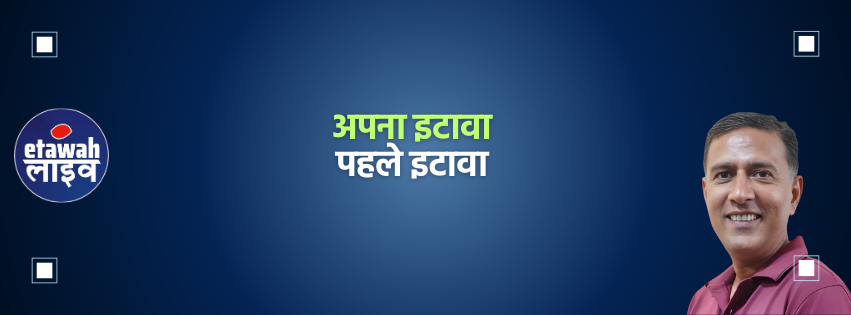1857 का साल… भारत की धरती क्रांति की आग में धधक रही थी। इटावा भी इससे अछूता नहीं था। हर गली, हर गाँव में आवाज़ गूँज रही थी—“फिरंगी भगाओ, आज़ादी लाओ।” इसी उथल-पुथल के बीच अंग्रेज मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ए.ओ. ह्यूम की हालत पतली हो गई थी।
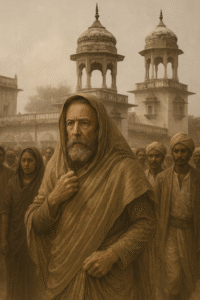
17 जून की सुबह खबर फैल चुकी थी कि विद्रोही अंग्रेज अफसरों पर धावा बोलने वाले हैं। ह्यूम जान गया कि अब उसकी बारी है। वह अब तक जनता पर राज करता था, लेकिन इस बार जनता उसकी जान लेने पर उतारू थी। मौत उसके दरवाज़े पर दस्तक दे रही थी। डर से काँपते ह्यूम ने वह कदम उठाया, जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी न की थी। उसने औरत का कपड़ा पहन लिया। एक देहाती महिला की तरह साड़ी और घूँघट ओढ़कर वह जनता की भीड़ में घुलने की कोशिश करने लगा। उसकी चाल और उसकी आँखों में छुपा डर साफ झलक रहा था।

सोचिए, वही ह्यूम जो किसानों को डरा-धमकाकर फैसले सुनाता था, वही आज भीड़ से छिपकर औरत का भेष धरकर भाग रहा था। यही अंग्रेजी राज की असलियत थी—बाहर से ताकतवर, अंदर से खोखले और डरपोक। वह धीरे-धीरे चलता हुआ बढ़पुरा पहुँच गया। उसे लगा कि यहाँ उसकी जान बच जाएगी। लेकिन किस्मत के पन्नों पर उसके लिए कुछ और ही लिखा था। गाँव के ठाकुरों और राजपूतों ने उसकी हरकतों पर शक कर लिया। उन्होंने घूँघट के पीछे छिपे चेहरे को पहचान लिया।
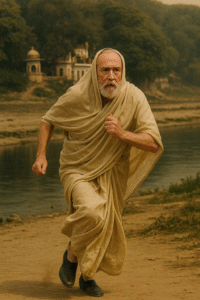
जैसे ही पहचान खुली, भीड़ भड़क उठी। लोग टूट पड़े उस पर। ह्यूम को पकड़कर बेरहमी से जूतों से पीटा गया। वह अंग्रेज अफसर, जो जनता के सिर पर राज करता था, आज उन्हीं के पैरों तले पड़ा था। हर वार में वर्षों का गुस्सा और अपमान छुपा था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। भीड़ का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग उसे वहीं खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन तभी गाँव के संभ्रांत लोग आगे आए। उन्होंने गुस्से में डूबे लोगों को समझाया—“इसे मारोगे तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाएँगे। छोड़ दो, ताकि दुनिया देखे कि हम भारतीय दयालु भी हैं।”

यही दया ह्यूम की जान बचा गई। लहूलुहान हालत में वह वहाँ से छूटकर फिर छिपने को मजबूर हो गया। लेकिन यह अनुभव उसकी आत्मा को हिला देने वाला साबित हुआ। इटावा में विद्रोह की आग सात दिनों तक जलती रही। चौकियाँ राख हो गईं, अंग्रेजों की सत्ता ध्वस्त हो गई और लोगों का गुस्सा आसमान छूने लगा। ह्यूम वहीं, छिपते-छिपाते अपनी सांसें गिन रहा था।

25 जून को ग्वालियर से ब्रिटिश फौज आई और इटावा पर दोबारा कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने झंडा तो फहराया, लेकिन जनता का गुस्सा उनकी नसों में डर बनकर बैठ चुका था। ह्यूम ने इन घटनाओं को भूला नहीं। अगस्त 1857 तक उसने एक रिपोर्ट तैयार की और अंग्रेज सरकार को भेज दी। उसमें उसने लिखा कि भारतीय समाज को केवल सैन्य बल से दबाना असंभव है। उनकी जातियों, उनके गुस्से और उनकी ताकत को समझना होगा।

उसने सुझाव दिया कि राजपूत, गुर्जर और अहीर जैसी जातियों को संसाधन दिए जाएँ ताकि वे सरकार के खिलाफ न खड़े हों। किसानों को साहूकारों और अदालतों से राहत दी जाए। लेकिन व्यापारियों और बनियों पर उसने टैक्स लगाने की सिफारिश की, क्योंकि उसके अनुसार वे केवल अपनी तिजोरी भरते थे। यह रिपोर्ट ह्यूम के भीतर के डर और अनुभव का नतीजा थी। वह समझ चुका था कि भारतीय समाज की ताकत को नज़रअंदाज़ करना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी।
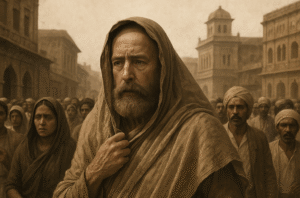
यही अनुभव आगे चलकर उसकी सोच की नींव बना। उसने महसूस किया कि भारतीयों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक मंच चाहिए। यही मंच आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। लेकिन इतिहास ने सब देख लिया। जिस अंग्रेज अफसर को जनता ने जूतों से पीटा था और दया दिखाकर छोड़ा था, वही आगे चलकर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का संस्थापक बना। यह विडंबना भी है और भारतीय ताकत का सबूत भी।

1857 का इटावा केवल विद्रोह की कहानी नहीं है। यह उस जनता की कहानी है जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। और यह उस अंग्रेज अफसर की कहानी भी है, जिसे औरत का भेष धरकर और जनता के पैरों तले पिटकर अपनी जान बचानी पड़ी।